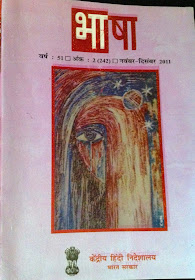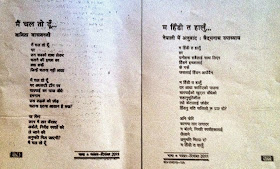हमदर्द की हिन्दी : कविता वाचक्नवी
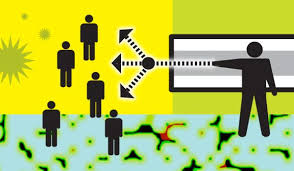
अपनी भाषा के प्रति हमदर्दी दिखाने के नाम पर दूसरी भाषाओं का मखौल उड़ाना अत्यंत हास्यास्पद और लज्जाजनक काम है। हिन्दी के दिखावटी हमदर्दों में यह प्रवृत्ति बहुत आम है कि वे हिन्दी को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अंग्रेजी का मखौल उड़ाते हैं। अंग्रेजी की शक्ति को कम करके आँकने से हिन्दी की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती अपितु उल्टे इस से हम हिन्दी वाले और मूर्ख ही प्रमाणित होते हैं।
अपनी भाषा के प्रति हमदर्दी दिखाने के नाम पर दूसरी भाषाओं का मखौल उड़ाना अत्यंत हास्यास्पद और लज्जाजनक काम है। हिन्दी के दिखावटी हमदर्दों में यह प्रवृत्ति बहुत आम है कि वे हिन्दी को श्रेष्ठ दिखाने के लिए अंग्रेजी का मखौल उड़ाते हैं। अंग्रेजी की शक्ति को कम करके आँकने से हिन्दी की श्रेष्ठता सिद्ध नहीं होती अपितु उल्टे इस से हम हिन्दी वाले और मूर्ख ही प्रमाणित होते हैं।
आज ऐसी ही एक और घटना देखी जब एक व्यक्ति ने प्रश्न उछला - "अगर शुभ रात्रि "GOOD NIGHT" होता है तो शुभ दीपावली "GOOD DEEPAWALI" क्यों नहीं ? या अगर शुभ दीपावली "HAPPY DEEPAWALI" होता है तो शुभ रात्रि "HAPPY NIGHT" क्यों नहीं ?"
उस पर उत्तर देने वालों ने लिखा - (1) "Because ...English is a very Funnnny language :)" और किसी ने लिखा "Kyunki Engligh Koi language nhi hai....jabardasti hi language haii"
यदि किसी भाषा के दो अलग अलग शब्दों का अनुवाद कोई अन्य भाषा अपने एक ही शब्द से करती है तो यह अनुवाद करने वाले की गलती है। Good और Happy दो अलग-अलग शब्दों को यदि दूसरी भाषा वाले एक ही अर्थ दे रहे हैं तो यह मूल भाषा की गलती कैसे हो गई, यह या तो अनुवादकों की गलती है या उनकी सुविधा।
हिन्दी के दो अलग अलग शब्दों को अंग्रेजी के किसी एक ही शब्द से अनूदित कर दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा ? यह हमारी समस्या या सुविधा है कि हम Haapy, Merry और Good तीनों के लिए 'शुभ' ही अर्थ लगा रहे हैं। .... और मजे की बात यह कि लोग हिन्दी से हमदर्दी दिखाने के नाम पर अंग्रेजी का मखौल उड़ा रहे हैं।
काश, इन्होंने संस्कृत पढ़ी होती तो भाषा के विकल्पों की जानकारी होती और अंग्रेजी के तीन अलग-अलग शब्दों के लिए कुछ अन्य पर्याय प्रयोग करना कम से कम जानते तो, और संस्कृत पढ़ी होती तो हिन्दी की शब्दावली में पर्यायों का अभाव है जैसा हिन्दी का मखौल भी न बनाते। फिर उसे जानने के बाद तो अंग्रेजी का यह मखौल बनाने का आधार ही समाप्त हो जाता। अस्तु !
कोई भी समझदार व्यक्ति अपनी भाषा की श्रेष्ठता दिखाने के लिए दूसरी भाषा का मखौल कभी नहीं उड़ाता। अंग्रेजी यदि हिन्दी की तुलना में कमतर है तो उसके पक्ष में यह बात हिन्दी वालों को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त है कि एक कमतर भाषा होने के बावजूद संसार के सारे अधुनातन ज्ञान-विज्ञान को वे अपनी भाषा में ले आए हैं, यह उस भाषा की शक्ति भी है कि वह उस सारे को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। दूसरी ओर हम लोग आज तक अपने यहाँ के उच्चशिक्षा के पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों तक को हिन्दी में नहीं ला सके हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति दूसरी भाषाओं का बहिष्कार नहीं करता क्योंकि स्वयं में कोई भी भाषा निकृष्ट या हास्यास्पद नहीं होती है वह एक बड़े भाषासमाज के सम्प्रेषण का सशक्त माध्यम होती है। फिर किसी बड़े भाषासमाज की भाषा का मखौल उड़ाना तो वस्तुतः अपनी मूर्खता या उथलापन प्रमाणित करना होता है।
किसी ने सच ही कहा है कि "जो दूसरे की माँ का सम्मान नहीं कर सकता, वह अपनी माँ का सम्मान स्वयं ही नष्ट कर देता है..."
आम तौर पर दिनों दिन अधिसंख्य लोगों के वैचारिक 'बरियर' और वैचारिकता के अभाव पर चकित रह जाना पड़ता है, इतना अधिक दिवालियापन है। इसका कारण उनकी जल्दबाज़ी नहीं लगता और न ही बोलने से पहले सोचना नहीं, अपितु सोचने की क्षमता और संस्कार कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुसंख्य समाज अब पढ़ता नहीं। स्वाध्याय बहुत आवश्यक होता है। पाती हूँ कि ऐसे लोग बड़े बड़े पदों पर हैं और ऐसी मूर्खता के साथ। तिस पर ये पद उनके अहंकार में और वृद्धि करते हैं । एक तो अज्ञान के कारण थोथा अहंकार और ऊपर से पद का अहंकार।
लोगों की दूसरी भाषाओं का अपमान करने की ऐसी मूर्खताओं के चलते ही भारत में हिन्दी के विरुद्ध वातावरण निर्मित होने में बड़ी भूमिका बनी। ऐसे लोग अंग्रेजी ही नहीं अपितु दक्षिण भारतीय भाषाओं या उत्तरपूर्व की भाषाओं का भी ऐसा ही अपमान करते चले आए हैं। जिसका परिणाम है कि भाषा के नाम पर देश बुरी तरह बंट चुका है और दूसरी भाषाओं के लोग भी इस कारण हिन्दी के विरोधी होते चले गए हैं।
किसी ने सच ही कहा है कि "जो दूसरे की माँ का सम्मान नहीं कर सकता, वह अपनी माँ का सम्मान स्वयं ही नष्ट कर देता है..."
हिन्दी से हमदर्दी दिखाने के दूसरे भी कई तरीके हैं, कई काम हैं। वैसे हिन्दी को ऐसी हास्यास्पद हमदर्दी की जरूरत भी नहीं है।